▪️महर्षि दयानन्द ने मतमतांतरों की आलोचना क्यों की?
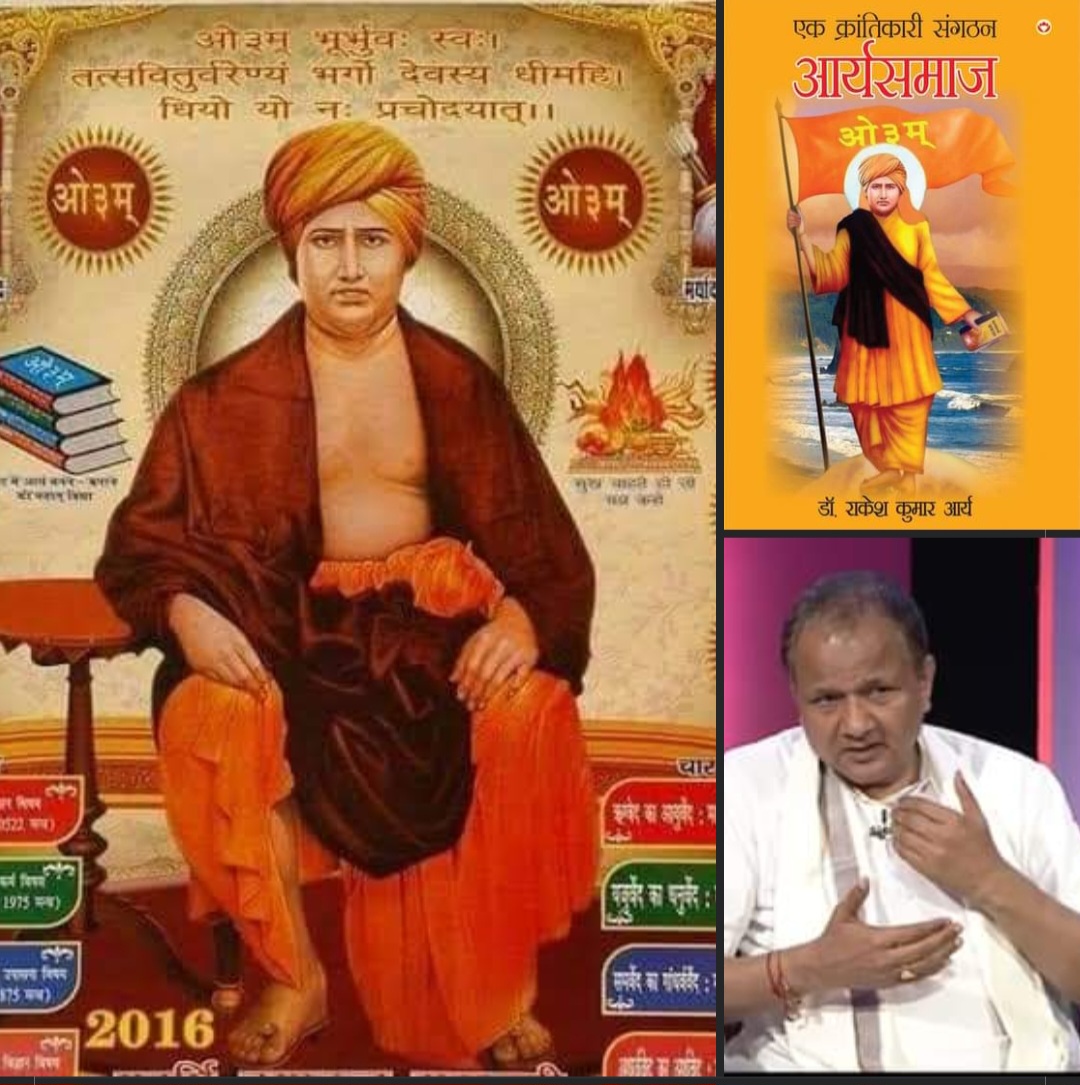
— स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती
ज्ञान का उल्टा मिथ्या ज्ञान या पाखण्ड है। “पाखण्ड” शब्द “पाषण्ड” शब्द का अपभ्रंश या विकृत रूप है। छद्म, छलयुक्त्त या कपट व्यवहार का नाम “पाषण्ड” है। कट्टर अप्रगतिशील हिन्दू को, जो जीवन के अभ्यन्तर में कुछ हो, और उसके विपरीत उसका बाह्य-आडम्बर साधु-सन्तों, भक्तों, धार्मिकों और विद्वानों जैसा हो, उसे भी पाषण्डी या पाखण्डी कहते हैं। स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ ‘सत्यार्थप्रकाश’ में पाखण्डी के समान पोप शब्द का भी एक रूढ़ि अर्थ किया है – पोप कौन है? स्वामी जी लिखते हैं – “इसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परन्तु अब छलकपट से दूसरे को ठग अपना प्रयोजन साधनेवाले को “पोप” कहते हैं। स्वामी जी ने पोप के समान सुन्दर शब्द को किस व्यंजना के कारण इस प्रकार की विकृत रूढ़िता दी, यह उनके शब्दों से स्पष्ट है – “सुना है जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे। बिना हमारी सेवा और आशा के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता; जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे, उतने की सामग्री तुमको स्वर्ग में मिलेगी, इत्यादि, इत्यादि।” पोप लोग हुण्डी लिखकर देते थे तो कबर में शव के सिर के नीचे रख दी जाती थी। पोपों की यह छद्मता बहुत दिनों तक यूरोप में चली। “जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी। पर अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई।” भारतवर्ष में हिन्दुत्व और धर्म के नाम पर घुलघुल करने वालों की संख्या कम नहीं है। स्वामी जी ऐसे ही व्यक्तियों को ‘पोप’ और पाखण्डी कहते है।
पोप और पाखण्डी के समान ही एक शब्द “धर्मध्वजी” है, जिसका प्रयोग मनुस्मृति में हुआ है। (४/१९५,१९६) पाखण्डियों के लक्षण बताते हुए ऋषि दयानन्द मनु के श्लोकों को उद्धृत करके कहते हैं – (धर्मध्वजी) जो धर्म कुछ भी न करे, परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, (सदा लुब्धः) सर्वदा लोभ से युक्त, (अधार्मिकः) कपटी, (लोक-दम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़ मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक, अन्य से बैर-बुद्धि रखने वाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको (वैडालव्रतिकः) विडाल के समान धूर्त और नीच समझे।
स्वामी जी आगे लिखते हैं – (अधोदृष्टिः) कीर्ति के लिए जो नीचे दृष्टि रखे, (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक, किसी ने उसका पैसा-भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे, (स्वार्थ साधना) चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो, परंतु अपना प्रयोजन साधने में चतुर, (शठः) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो, परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ-मूठ ऊपर से शील-सन्तोष और साधुता दिखलावे, उसको (वकव्रतः) बगुले के समान नीच समझो। ऐसे-ऐसे लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं, उनका विश्वास वा सेवा कभी न करे।’
मनुस्मृति के इन श्लोकों में जिस पाखण्ड का उल्लेख है वह व्यक्तिगत है। कोई एक व्यक्ति पाखण्डी, धर्मध्वजी, दंभी, कपटी या छद्मी हो तो उससे समाज की उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि उन संस्थाओं, मतमतान्तरों या सम्प्रदायों द्वारा होती है जिनका आधार छल-छद्म, कपट, अन्ध-विश्वास, स्वार्थ-परायणता और पाखण्ड है।
प्राचीनतम वैदिक युग में मनुष्य का एक स्वाभाविक धर्म था जो परमात्मा के प्रेम और प्रकृति, जीव और सृष्टि नियंता के सहज सम्बन्ध पर निर्भर था। समय बदला, मनुष्य की दुर्बलतायें स्वार्थ की श्रृंखला में बंध गयीं, वैमनस्य आरम्भ हुए और नैतिकता का ह्रास हुआ। मनुष्य का विश्वास ईश्वर पर न रहा। ऐसे समय में अनीश्वरवाद का प्रचार हुआ और मनुष्यता का पतन। अनीश्वरवादियों ने दुर्बल मनुष्य को ही अपना आराध्य माना। मूर्तियों, मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों, पीरों, पैगम्बरों, मसीहों और अवतारों का युग आया। धरती का स्वर्ग आसमान में उड़ गया। पाखण्डियों ने उस स्वर्ग तक पहुंचाने के धन्धे आरम्भ किये। धर्म के जिस मार्ग को छुरे की धार या दुर्गम पथ कहा जाता था (क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति) स्वार्थियों ने उसके सस्ते धंधे आरम्भ किये। ऐसे समय में ही १८७४ में स्वामी दयानन्द ने अपना अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश लिखा, जिसमें उन्होंने वैदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के अनन्तर चार समुल्लासों में साम्प्रदायिक विचारधारा की आलोचना की।
(स्रोत: डॉ. भवानीलाल भारतीय कृत “भारतवर्षीय मतमतान्तर समीक्षा” की भूमिका, पृ.८-९)








